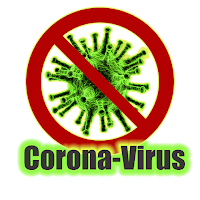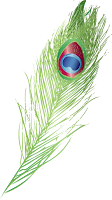बीती ताहि बिसार दे

स्मृतियों का दामन थामें मन कभी-कभी अतीत के भीषण बियाबान में पहुँच जाता है और भटकने लगता है उसी तकलीफ के साथ जिससे वर्षो पहले उबर भी लिए । ये दुख की यादें कितनी ही देर तक मन में, और ध्यान में उतर कर उन बीतें दुखों के घावों की पपड़ियाँ खुरच -खुरच कर उस दर्द को पुनः ताजा करने लगती हैं। पता भी नहीं चलता कि यादों के झुरमुट में फंसे हम जाने - अनजाने ही उन दुखों का ध्यान कर रहे हैं जिनसे बड़ी बहादुरी से बहुत पहले निबट भी लिए । कहते हैं जो भी हम ध्यान करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है और इस तरह हमारी ही नकारात्मक सोच और बीते दुखों का ध्यान करने के कारण हमारे वर्तमान के अच्छे खासे दिन भी फिरने लगते हैं । परंतु ये मन आज पर टिकता ही कहाँ है ! कल से इतना जुड़ा है कि चैन ही नहीं इसे । ये 'कल' एक उम्र में आने वाले कल (भविष्य) के सुनहरे सपने लेकर जब युवाओं के ध्यान मे सजता है तो बहुत कुछ करवा जाता है परंतु ढ़लती उम्र के साथ यादों के बहाने बीते कल (अतीत) में जाकर बीते कष्टों और नकारात्मक अनुभवों का आंकलन करने में लग जाता है । फिर खुद ही कई समस्याओं को न्यौता देने...